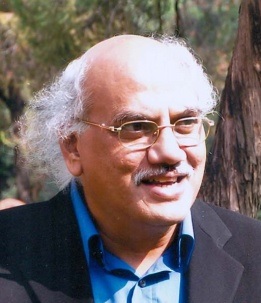संतोष चौबे
वर्ष 2019 में भारत की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल से प्रारंभ हुआ ‘विश्व रंग’ टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव अब विश्व के 65 से अधिक देशों तक विस्तारित हो चुका है। भारत, मॉरीशस और श्रीलंका से घूमते हुये वह एक बार फिर भोपाल में है जहाँ 27 से 30 नवंबर के बीच रवींद्र भवन परिसर में इसका आयोजन किया जायेगा।
ये शायद देश में पहली बार है कि कोई शैक्षिक संस्थान – रबींद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय एवं डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय – इस तरह का साहित्य एवं कला महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। देश में आयोजित होने वाले कई अन्य साहित्य उत्सवों के बदले विश्व रंग हिंदी और भारतीय भाषाओं को कैंद्रीयता प्रदान करता है। एक ओर तो यह हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच आपसदारी और परस्पर सम्मान का रिश्ता कायम करना चाहता है तो दूसरी ओर बोलियों से भी एक रसभरे संवाद की शुरुआत करना चाहता है।
आइये देखते हैं विश्व रंग की मूल अवधारणाएँ क्या हैं। विश्व रंग की अवधारणा, विश्व के बारे में हमारी समझ से ही निकलती है। यदि आप सचेत रूप से अपने आस-पास देखें तो पाएंगे कि विकास की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है और प्रकृति का जिस तरह अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है वह स्वयं हमारे अस्तित्व के लिये ही घातक होता जा रहा है। दूसरी ओर बायोटेक्नॉलॉजी एवं बायो इनफर्मेटिक्स के कन्वर्जेंस से जिस तरह के मनुष्य के निर्माण की बात की जा रही है उससे इस बात में भी संदेह पैदा होता है कि क्या मनुष्य स्वयं वैसा बचा रह पाएगा जैसा कि हम उसे जानते हैं। तीसरे, टेक्नॉलॉजी ने जीवन की गति इतनी तेज कर दी है कि उसे जानना-पहचानना ही मुश्किल होता जा रहा है। हमें जीवन को समझने के लिये नये नक्शों और नये को-आर्डिनेट्स की तलाश करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। मुझे लगता है कि जीवन के नये उपकरणों को तलाशने के साधन विज्ञान के पास उतने नहीं हैं जितने कला, संस्कृति और संगीत के पास हैं। उनमें भी भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्व के तमाम रचनाकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों को इस संबंध में बातचीत शुरु करनी चाहिये और एक प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिये। विश्व रंग इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
विश्व रंग साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भाषा में काम करने वाले रचनाकारों के बीच वैश्विक विमर्श की शुरुआत है। देश और विदेश के लगभग 100 विश्वविद्यालय एवं संस्थायें इसमें शामिल हैं, जिनमें आपसी बातचीत एवं शैक्षणिक नेटवर्क का निर्माण इस कार्यक्रम का बड़ा हासिल होगा। देशभर से लगभग 1000 शीर्षस्थ रचनाकार इसमें शिरकत करते रहे हैं, और उम्मीद है कि उनके बीच संवाद का रिश्ता कायम होगा और सबसे बढ़कर, हिन्दी और भारतीय भाषाओं को केन्द्रीयता प्रदान करने का प्रयत्न किया जायेगा।
वनमाली सृजन पीठ और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का जो लगभग 35 वर्षों का साहित्य एवं कलाओं में काम करने का अनुभव है वह बताता है कि अंततः सभी कलाओं और अनुशासनों में एक तरह की आपसदारी बनती है और उसे पहचानना ही अपने कलात्मक क्षितिज का विस्तार करना है। इसी तरह अन्य अनुशासन भी कलात्मक विधाओं में हस्तक्षेप करते हैं। मसलन उपन्यास और कहानी में कई समकालीन तथा युवा रचनाकारों के यहां आपको ऐसी शैलियों और अनुशासनों की छाया मिल जायेगी जिन्हें पहले उपन्यास या कहानी के डोमेन में नहीं रखा जाता था, उनमें आप इतिहास की, चित्रकला की, फिल्म तकनीक की, नाटक की और दार्शनिक निष्कर्षों की छाया पाते हैं। असल में ज्ञान-विज्ञान का जो विस्फोट हमारे आसपास हुआ है, उसने बहुत सारी पुरानी सीमा रेखाओं को तोड़ा है। उपरोक्त सभी अनुशासनों को विभिन्न सत्रों को आयोजन में शामिल करने का लक्ष्य इस नये उभरते मानचित्र को पहचानना है।
`विश्व रंग’ पॉपुलर सब्जेक्ट्स या लोकप्रिय को खारिज नहीं करता बल्कि पॉपुलर और अकादमिक सत्रों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जहां एक ओर लोक और शास्त्र, शिक्षा और विज्ञान और भाषाओं पर केन्द्रित सत्र हैं तो दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुशायरा, उर्दू की रवायत में सुखन की महफिल और पॉपुलर बैंड्स भी हैं जो युवाओं के लिये आकर्षण का केन्द्र हैं। यहाँ तक कि अकादमिक सत्रों में भी लीक को छोड़कर थर्ड जेंडर तथा दिव्यांग कवियों का कविता पाठ, सोशल मीडिया पर सक्रिय रचनाकार तथा लेखक से मिलिए में साहित्य, संगीत और फिल्म के रचनाकार हैं जो हिन्दी के वरिष्ठ रचनाकारों के साथ प्रस्तुत होते हैं।
जैसे साहित्य ने अपने आप को जमीन से काटकर बड़े शहरों पर केन्द्रित कर लिया है, वैसे ही स्थापित कला दीर्घाओं में भी व्यावसायिकता हावी है और उभरते चित्रकारों के लिये, जो गांव, कस्बों और दूरदराज के स्थानों से आते हैं कोई जगह नहीं है। हमारी कोशिश है कि उन्हें पहचाना जाए और उन्हें प्रदर्शित किया जाए। जिस तरह का रिस्पांस इस प्रयास को मिला है, वह बताता है कि इन कलाकारों में किस तरह की छटपटाहट है। करीब एक हजार से अधिक प्रविष्टियां हमें विश्व रंग नेशनल पेंटिंग एक्ज़िविशन के लिये प्राप्त हुई हैं जिनके रंगों और आकृतियों के प्रयोग अद्भुत, अछूते एवं अनोखे हैं। यह कला की दुनिया में एक नया प्रयोग है। देश के दिग्गज चित्रकारों पर मोनोग्राफ्स का प्रकाशन विश्व रंग की विशेषता है जिनमें ए.जी. रामचंद्रन, अफज़ल तथा नैनसुख जैसे अछूते चित्रकार शामिल हैं भारतीय चित्रकला में नारी परिप्रेक्ष्य, कला में अमूर्तन जैसे विषयों पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किये गये हैं। विश्व रंग 2025 में बच्चों के लिये चित्रकला प्रतियोगिता तथा वर्कशॉप का अलग से आयोजन किया जा रहा है जिसमें भोपाल की विभिन्न शालाओं के 1000 से अधिक बच्चे शामिल होंगे।
ये फेस्टिवल टैगोर की रचनात्मकता से शुरु होकर पूरे विश्व तक फैलता है। हमारे तो विश्वविद्यालय का नाम ही गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है और ये हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है। जैसे-जैसे हम काम करते हैं तो पाते हैं कि लगभग पूरे हिन्दी भाषी क्षेत्र में टैगोर की विराट रचनात्मकता, विशेषकर उनकी पेंटिंग स्टाइल एवं नाटकों को लेकर कोई बहुत चेतना नहीं है और इसका पुनरावलोकन आवश्यक है। विशेषकर टैगोर और गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन के समय का रिश्ता और टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयता तथा शैक्षिक दृष्टि को एक बार फिर से देखा जाना ज़रूरी है। हमारा दूसरा वैचारिक आधार भाषाई विमर्श पर आधारित है। आप देखिये कि राजनीति ने हमारे देश में सारी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम किया जबकि वे सहोदर हैं और एक-दूसरे से बड़ी ताकत पा सकती हैं। वैसे ही बोलियों को भी हिन्दी के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास है जबकि स्वयं हिन्दी भाषा अपना रस इन जीवन सिक्त बोलियों से ही प्राप्त करती है। अतः बोलियों और भाषाओं पर सत्र रखे गये हैं जोकि हमारी उपरोक्त अवधारणाओं को अभिव्यक्त करेंगे।
जब हम भारतीयता पर जोर देते हैं तो ये कोई जड़ राष्ट्रीयता नहीं है। हमारी भारतीयता वैश्विक संदर्भों से जुड़ी और अपने अनोखेपन में प्रकाशित भारतीयता है जिसमें विश्व कविता का भी उतना ही स्थान है जितना भारतीय कविता का। ये शायद पहली बार होगा कि किसी फेस्टिवल में विश्व कविता के दो सत्र आयोजित हैं। इसी तरह प्रवासी भारतीय लेखक भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन उनके लेखन के प्रकाशन और मूल्यांकन को लेकर कोई ठोस प्रयास देश में नहीं होते। विश्व के प्रमुख प्रवासी भारतीय लेखकों को आमंत्रित करने का लक्ष्य है कि उनसे संवाद कायम किया जाये एवं उनके साहित्य के मूल्यांकन के प्रयास किये जायें। इस समय भारत के बाहर करीब 100 से अधिक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है। इनके साथ सहयोगी वातावरण बन सके इसलिये इन्हें भी आमंत्रित किया गया है। अंततः वैश्विक हिन्दी के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका होगी।
दस्तावेजीकरण विश्व रंग का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। विश्व रंग 2025 तक आते-आते कई ऐसे प्रयास किये गये हैं जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदी की लगभग 200 वर्षों की कथा परंपरा को समेटते हुये, 600 से अधिक कथाकारों तथा आलोचकों के साथ, 18 खंडों में `कथा देश’ का प्रकाशन, अविभाजित मध्यप्रदेश के कथाकारों को समेटते हुये 6 खंडों में `कथा मध्यप्रदेश’ का प्रकाशन और भोपाल के 171 कथाकारों के साथ `कथा भोपाल’ का प्रकाशन दस्तावेजीकरण के ऐसे ही महती प्रयास हैं। हिंदी में विज्ञान कथाओं की ज़रूरत को महसूस करते हुये 6 खंडों में `विज्ञान कथा कोश’ एवं तीन खंडों में ‘विज्ञान कविता कोश’ का प्रकाशन भी किया गया है। बच्चों की दुनिया को समृद्ध बनाते हुये 11 खंडों में `बाल कविता कोश’ भी अब प्रकाशित है। विश्व रंग 2025 में अब 20 खंडों में ‘काव्यदेश’ का प्रकाशन भी किया जा रहा है। विश्व के 65 देशों में हिंदी की स्थिति को लेकर ‘विश्व में हिंदी’ रिपोर्टट का लोकार्पण भी इस समारोह में किया जायेगा।
`विश्व रंग’ के अंतर्गत अब चार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। जहाँ `विश्व रंग’ पत्रिका वैश्विक संदर्भों को समेटती त्रैमासिक पत्रिका है वहीं `वनमाली’ कथा केंद्रित पत्रिका है जिसने थोड़े ही समय में `कथा विश्व’ में अपना स्थान बनाया है। कला पर केंद्रित `रंग संवाद’ पिछले बारह वर्षों से प्रकाशित है तो हिंदी में विज्ञान विषयों पर केंद्रित पत्रिका `इलेक्ट्रॉनिकी’ देश की एकमात्र पत्रिका है जो पैंतीस से अधिक वर्षों से प्रकाशित है। अब ऑनलाइन पत्रिकाओं और समूहों ने भी अपना स्थान बनाया है। `अनन्या’ करीब दस देशों से, `साझा संसार’ नीदरलैंड्स और यूरोप के अन्य देशों से, `भारत दर्शन’ न्यूज़ीलैंड से ऑनलाइन प्रकाशित है। भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में कई ऑनलाइन समूह कार्य कर रहे हैं जो सालभर में 100 से अधिक संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। ऑनलाइन प्रकाशनों, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
विश्व रंग 2025 की एक और विशेषता बच्चों के लिये एक पूर्ण कालिक समानांतर `बाल विश्व रंग’ का तथा मानव संग्रहालय के सहयोग से `आदिवासी साहित्य तथा कला महोत्सव’ का आयोजन है जो विश्व रंग में नये रंग भरने का काम करेंगे।
इस फेस्टिवल के पहले देश के 500 स्थानों पर पुस्तक यात्राऐं आयोजित की गई थीं। जिस तरह हमारे गांव व कस्बों ने पुस्तक यात्राओं को हाथों-हाथ लिया उससे उम्मीद बनती है कि पुस्तक संस्कृति अभी हमारे देश में जीवित है। बच्चे और युवा किताबें पढ़ना चाहते हैं, हम ही उन तक नहीं पहुंच पाते। पुस्तक यात्रा इस भ्रम को तोड़ती है कि किताबों के पाठक कम हो रहे हैं। वो बताती है कि किताबें अब भी बातें करती हैं, और व्यापक भारतीय समाज में ज्ञान की भूख अभी बरकरार है। हम अगले एक साल में एक लाख से अधिक पुस्तक मित्र बनाने का प्रयास करेंगे।
आईसेक्ट के सभी विश्वविद्यालय और पूरा आईसेक्ट नेटवर्क ‘विश्व रंग’ के आयोजन में शामिल है।
आईसेक्ट आज देश का लगभग सबसे बड़ा सामाजिक उद्यमिता आधारित नेटवर्क है और वह समाज के पास जाने में विश्वास रखता है। आईसेक्ट इस पूरे प्रयास को एक सामाजिक जरूरत के रूप में देखता है और सामाजिक उद्यमिता द्वारा इसकी पूर्ति करना चाहता है।
तेजी से बदलते समय में कोई भी भविष्य की घोषणा नहीं कर सकता पर विश्व रंग एक ऐसी रचनात्मक समावेशी प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहता है, जिसमें कलाएं मानव व मानवीय संवेदनाओं के पक्ष में खड़ी हों, सस्टेनेबल डेव्लपमेंट हमारी चिन्ता के केन्द्र में हो और हिन्दी और भारतीय भाषाओं को विश्व में उचित स्थान मिले, रचनात्मक विस्तार की जगह मिले। राष्ट्र के भीतर उनमें आदान-प्रदान बढ़े। आगे भी हमारी कार्यवाही का आधार उपरोक्त अवधारणायें ही होंगी। विचार के साथ-साथ हम एक्शन पर भी बल देते हैं। इसी से आगे के रास्ते प्रकाशित होंगे।